 |
| Solid Waste In Hindi |
⭐ Important for :
- Prelims (सामान्य अध्ययन : प्रश्न पत्र - 1)
- Mains (सामान्य अध्ययन - 3)
💭 ठोस अपशिष्ट क्या है?
ऐसा अपशिष्ट/कचरा जो ठोस अवस्था में हो और आर्थिक उपयोग के लिए प्रयोग में लाने योग्य न हो ठोस अपशिष्ट (Solid Waste) कहलाता है। ठोस अपशिष्ट के अधिक बढने का कारण आधुनिकीकरण एवं शहरीकरण है। ठोस अपशिष्ट एक वैश्विक समस्या है जिसके निस्तारण की आवश्यकता होती है। बढ़ते अपशिष्ट प्रदूषण के लिए मुख्य जिम्मेदार घटक 'प्रयोग करो और फेकों संस्कृति' है।
📊 भारत में ठोस अपशिष्ट (Solid Waste in India)
1947 के समय भारत में सालाना 6 मिलियन टन ठोस कचरा निकलता था किन्तु आधुनिकीकरण/शहरीकरण के बाद वर्तमान भारत में 2019 के आकड़ों के अनुसार अब यह बढ़कर 68.8 मिलियन टन हो चुका है अर्थात लगभग 11 गुना बढ़ गया है। इनमें से लगभग 7 मिलियन टन खतरनाक अपशिष्ट (Hazardous Waste) भारत में प्रत्येक वर्ष उत्पन्न होता है जो कि स्वास्थ्य के लिए अत्यंत ही हानिकारक होता है। भारत में औसतन 500 ग्राम/व्यक्ति प्रतिदिन ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है।
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम - 2016
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम -2016 [Solid Waste Management (SWM) -2016] , वर्ष 2000 के 'म्युनिसिपल ठोस अपशिष्ट नियम' का संशोधित रूप है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 के अनुसार इकट्ठा किए गए स्थान पर ही ठोस एवं गीले अपशिष्ट को अलग कर देने का प्रावधान है। इस नियम के अंतर्गत सम्पूर्ण अपशिष्टों को तीन रूपों में वर्गीकृत किया गया है - जैव निम्नीकरण, गैर-जैव निम्नीकरण और घरेलू खतरनाक अपशिष्ट
इस नियम के अंतर्गत स्थानीय निकायो जैसे नगरपालिका आदि को उत्तरदायित्व दिये गए है जिसमे घर-घर से कचरा संग्रहण, वर्मी कंपोस्टिंग, बायोमिथनेशन आदि शामिल है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम के अनुसूची-1 एवं 6 में 'खतरनाक एवं अन्य अपशिष्ट नियम-2016' का उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत खतरनाक पदार्थों के लिए कुछ कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है। ये निम्न है -
- न्यूनीकरण (Minimization)
- पुनः प्रयोग (Reuse)
- पुनर्चक्रण (Recycle)
- निवारण (Prevention)
- सुरक्षित निस्तारण (Safe Disposal)
- रिकवरी, उपयोग और प्रसंस्करण (Recovery, Utilization and Co-processing)
ठोस अपशिष्ट के प्रभाव (Effect of Solid Waste)
🌿 पर्यावरण पर प्रभाव
अपशिष्टों के माध्यम से हानिकारक मिथेन गैस का निर्माण होता है जो की वैश्विक तापन (ग्लोबल वार्मिंग) के लिए जिम्मेदार गैसों मे से एक है। कचरे का अवैध निपटारा भी पर्यावरण के लिए अत्यंत हानिकारक है। प्लास्टिक जैसे ठोस अपशिष्ट मृदा के उपजाऊ क्षमता को कम करते है।
👫मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव
ठोस अपशिष्ट मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है इनका मानव जीवन पर प्रभाव प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में है। जब ये अपशिष्ट जलते है तो वायु को जहरीला बना देते है जिससे मानव स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इन अपशिष्टों के कारण कैंसर रोग होने का भी खतरा होता है। पारा (मर्करी), लेड, आर्सेनिक जैसे तत्व अपशिष्ट के रूप में जल में घुलते है और मानव के लिए खतरा उत्पन्न कर देते है।
🐃 जानवरों एवं जलीय जीवन पर प्रभाव
ठोस अपशिष्टों से निकला मर्करी जल में घुलकर उसे विषैला बना देता है जिससे मछलियों और अन्य जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है। सड़कों पर फैले अत्यंत हानिकारक ठोस अपशिष्टों जैसे प्लास्टिक मटेरियल को पशुएँ (Animals) निगल जाते है जिससे उनके जान को खतरा हो जाता है। प्लास्टिक ट्यूब का अत्यधिक बुरा प्रभाव जलीय जीवों को होता है, ये जल की गुणवत्ता में कमी करके उसे दूषित बना देते है।
ठोस अपशिष्ट समस्या के कारक
ठोस अपशिष्ट समस्या का मुख्य कारण तीव्र शहरीकरण, जीवन पद्धति (Lifestyle) में परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि, जागरूकता न होना, अपर्याप्त सरकारी नीतियाँ आदि है।
ठोस अपशिष्ट का उपचार (Treatment of Solid Waste)
🔥 भस्मीकरण (Incineration)
ठोस अपशिष्टों के निपटारे के लिए भस्मीकरण वह विधि है जिसमे ठोस कचरों को 1000° C पर जलाया जाता है, यह एक व्यावहारिक विधि है जो की कचरा निपटारे के लिए समान्यतः प्रयोग में लाया जाता है किन्तु स्वास्थ्य की दृष्टि से यह विधि खतरनाक है इसमें अपशिष्टों के जलने के दौरान निकले विषैले गैस जो की वायुमंडल में मिलती है मानव स्वस्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है।
🍞 भूमि भराव (Land Fills)
नगर के बड़े गड्ढों को भरने के लिए पहले ठोस अपशिष्टों का भराव करते है फिर पूरा भर जाने के बाद इसके ऊपर मिट्टी डालकर इसे समतल कर लेते है। यह एक सस्ता विधि है किन्तु इसका उपयोग एक स्थान पर हो जाने के बाद दुबारा नहीं किया जा सकता तथा इससे भूमिगत जल भी प्रदूषित होता है।
💦 समुद्री डंपिंग (Ocean Dumping)
इसमें अपशिष्ट को समुद्री जलमग्न तट पर डंप किया जाता है। किन्तु यह भी तरीका पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
💥 ताप-अपघटन (Pyrolysis)
इस प्रक्रिया में ऑक्सीज़न की अनुपस्थिति में ठोस अपशिष्टों का दहन किया जाता है। कार्बनिक अपशिष्टों के तापीय अपघटन से टार, चारकोल और एसीटोन जैसे पदार्थों का उत्पादन होता है। अधिकतर बड़े शहरों में ऐसे संयंत्र लगे होते है।
🍀 जैविक पुनर्प्रसंस्करण (Biological Reprocessing)
इस विधि में खाद्य अपशिष्टों, पौधो के रूखे-सूखे मलवे और कागज अपशिष्टों को अपघटक के माध्यम से कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते है।
💢 वर्मीकल्चर (Varmiculture)
इस विधि में केचुओं (Earthworm) का प्रयोग किया जाता है। अपशिष्ट पदार्थों में इन केचुओं को मिलाया जाता है जो अपशिष्टों को तोड़कर मल उत्सर्जन द्वारा पोषक तत्वों में परिवर्तित कर देते है।
3R's (Reduce-Reuse-Recycle)
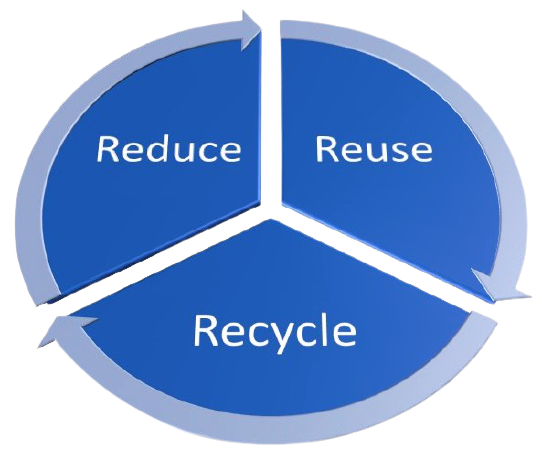 |
| Reduce (निम्नीकरण) - Reuse (पुनर्प्रयोग) - Recyle (पुनर्चक्रण) |
- Reduce अर्थात न्यूनीकरण से तात्पर्य है कि मानव को पदार्थों का आवश्यकता से अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए।
- पुनर्प्रयोग (Reuse) से तात्पर्य है कि मानव को वस्तुओं को फेकने के स्थान पर पुनः उपयोग में लाना चाहिए।
- पुनर्चक्रण (Recycle) से तात्पर्य है कि पदार्थों को पुनः नए उत्पादों में बदलकर उपयोग में लाना चाहिए।
⭐ Note : यह लेख Prelims के साथ-साथ Main (GS-3) - Ecology के लिए भी महत्वपूर्ण है।
Note: 📢










